वाटरशेड: भारत के पानी को हमने किस तरह से नष्ट किया और हम कैसे इसे बचा सकते हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन पर मृदुला रमेश के काम का एक शानदार वर्णन है।
परिचय में उन्होंने क्लाइमेट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक पॉल डिकिंसन को उद्धृत किया है, जिन्हें यह कहने का श्रेय दिया जाता है, “यदि जलवायु परिवर्तन एक शार्क है, तो पानी उसके दांत हैं।”
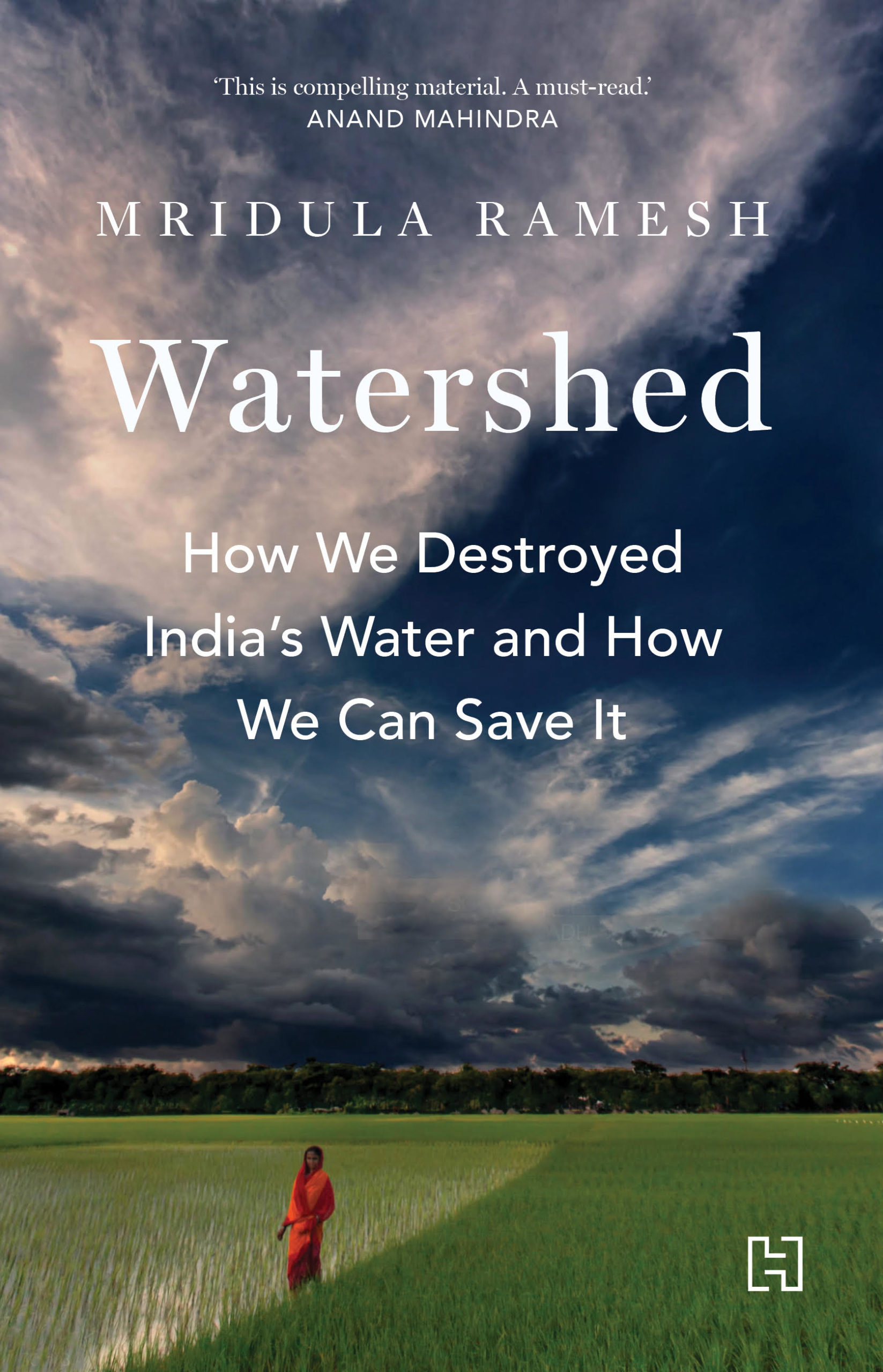
यह उद्धरण उनके लिए है, जो केवल समरूपता की शक्ति पर जोर देते हैं और यह दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन का तत्काल प्रभाव, पानी से संबंधित आपदाएं- बाढ़, सूखा और बड़े पैमाने पर बहु-आयामी आपदाएं, जैसे, भूस्खलन को बढ़ाने वाली हिमनद झील से होने वाली बाढ़- हैं। जलवायु परिवर्तन की यहां मौजूदगी है, और भारत पहले से ही इसका दंश महसूस कर रहा है।
रमेश की पुस्तक आंशिक इतिहास है, आंशिक उपाख्यान है और आंशिक परिवर्तन के लिए नसीहत है। इसमें अंतर्निहित शोध, इसे विशेष शक्ति देता है, और वह अपनी कहानियों को सावधानी से चुनती हैं। शुरुआती अध्याय विज्ञान से संबंधित हैं, जो मानसून की कहानियां और इसकी परिवर्तनशीलता के कारण बताते हैं; सूखे, चक्रवात और देश में जलवायु आपदाओं के प्रभाव के बारे में बताती हैं, जहां पानी की उपलब्धता बारिश पर निर्भर है।
इतिहास के वाटरशेड से संबंधित सबक को भुला दिया गया
इसका दायरा ऐतिहासिक रूप से विशाल है। यह किताब सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन शहर पाटलिपुत्र दोनों के पतन के पीछे सूखे और बाढ़ को बताती है। इस तरह यह एक मजबूत अंतर्दृष्टि देती है कि पानी एक ऐसी शक्ति है जो सभ्यताओं के अंत का कारण बन गई। मृदुला रमेश बताती हैं कि कैसे शोध से पता चलता है कि इनके पतन का कारण, गर्मियों के मानसून का 200 वर्षों से कमजोर होना रहा। उत्तरार्द्ध के पतन का कारण लगभग 17 दिन में लगातार बारिश का होना था, जिससे नदियों से घिरा एक राज्य कमजोर होता गया। उनका कहना है कि इन दोनों सभ्यताओं ने प्रभावी जल प्रबंधन से, अपने को ताकतवर बनाया, लेकिन तबाही के सामने मानवीय चतुरता की सीमाएं हैं। बहरहाल, वाटरशेड मुख्य रूप से इस बारे में है कि कैसे देखभाल और मानवीय चतुरता, कम से कम, एक हद तक, एक आपदा का प्रबंधन कर सकती है।
उनका सुझाव है कि भारत के वाटरशेड प्रबंधन में हमारी वर्तमान समस्याएं प्रबंधनीय हैं। भारत आत्म-सुधार कर सकता है। भारत को आंकड़े एकत्र करने हैं, अपनी ताकत का एहसास करना है और जल प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण तत्वों- जंगल, वाटर टैंक (एक शब्द जो दक्षिण एशिया में छोटे जल निकायों को संदर्भित करता है) और अपशिष्ट जल प्रबंधन, को सक्रिय रूप से मजबूत करना है, ये सभी आगे का राह तय करते हैं।
खेती की जमीन के लिए जंगल साफ करने के मामले में, मृदुला रमेश, मुगल भूमि प्रबंधन के साथ एक छोटे विराम और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ बड़े विराम की पहचान करती हैं। इसमें वह आंशिक रूप से ही सही हैं। कुछ मुद्दों का लंबा इतिहास है। जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिक प्रकाश काशवान ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन द वुड्स: एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया, तंजानिया एंड मैक्सिको में उल्लेख किया है कि वनों के प्रबंधन का आकार सदियों से निराशाजनक रूप से समान है। 400 बीसीई और 200 सीई के बीच लिखी गई मनुस्म़ृति में, “भूमि को खाली करने वाले लोगों के लिए पहले कब्जे के पवित्र अधिकार की घोषणा है, भले ही उन्होंने दूसरों से, उदाहरण के लिए, शिकारी और पशुचारक, भूमि लेकर उसका उपयोग किया हो।”
17वीं शताब्दी के मुगल बादशाह औरंगजेब ने घोषणा की कि “जो कोई भी (बंजर भूमि) को कृषि योग्य भूमि में बदल देता है उसे (स्वामी) के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उसे (भूमि से) वंचित नहीं किया जाना चाहिए।”
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में एक बड़ा विराम, भूमि प्रबंधन प्रथाओं के कारण नहीं, बल्कि उनके शासन के तरीके के कारण संभव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी (स्पष्ट कारणों से) और ब्रिटिश राज, दोनों स्थिरता के बजाय, लाभ कमाने पर केंद्रित थे। मृदुला रमेश, 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर के विचारों की बात करती हैं कि भारत को यूरोपीय लोगों द्वारा “बेहतर प्रबंधित” किया जा सकता है। साथ ही साथ, यह भी बताती हैं कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य में ‘मुक्त व्यापार’ न तो उचित था और न ही मुक्त था। औपनिवेशिक प्रथाओं ने वन भूमि और पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्रभावित किया, इसका एक बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए, डेन हकलब्रिज की पुस्तक ‘नो बीस्ट सो फियर्स: द टेरिफिंग ट्रू स्टोरी ऑफ द चंपावत टाइगर, द् डेडलियस्ट मैन-ईटर न हिस्ट्री’ है।
आदमखोर बाघों की संख्या बढ़ने जैसी स्थितियों के उद्भव पर फोकस करते हुए, हकलब्रिज की किताब बताती है कि नेपाल और भारत में पारिस्थितिक प्रबंधन में पिछली प्रथाएं, शासकों और ऐसे विषयों पर आधारित रहीं, जिनमें वनों (और बाघों) को चिह्नित करने की प्रक्रिया ने ‘विकास’ की प्रकृति को उलट दिया। इसका आधार प्रकृति को नियंत्रित करना और जितना संभव हो उतना अधिक धन निकालना रहा, जिससे पारिस्थितिक तबाही हुई।
अमीर फसलें, गरीब किसान, दीवालिया वाटरशेड्स
वाटरशेड में बताया गया है कि किस तरह से करों को, उत्पादन में, उतार-चढ़ाव से अलग करके, फसल के अनुपात के बजाय, नकद राजस्व के रूप में निश्चित किया गया और इसका केंद्रीकरण किया गया जिसने भारतीय कृषि को गहरे तक प्रभावित किया।
उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों की उपज की शुरुआत हुई। इनमें से कई ऐसी फसलें थीं, जो उन जलवायु के लिए अनुपयुक्त थीं जिनमें वे उगाई जाती थीं। रेलवे के माध्यम से इन फसलों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक हुई। इनकी वजह से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और बांधों व नहरों के माध्यम से प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए एक तकनीकी जुनून पैदा हुआ। इस प्रक्रिया में, बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया (जिससे मानव-पशु संघर्षों में वृद्धि हुई, जैसा कि नो बीस्ट सो फियर्स में दिखाया गया है), स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन की उपेक्षा की गई, और स्थानीय निर्णय लेने की स्थिति को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अधीन कर दिया गया।
आजादी के बाद भारत ने एक हद तक इस रास्ते पर चलना जारी रखा है। प्रधानमंत्री के रूप में, अपने पहले भाषण में, 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्रता “पूरी तरह से या पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि बहुत हद तक” प्राप्त की गई है। ‘पूर्ण रूप में नहीं’ में देश द्वारा शुरू की जाने वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल थीं; जिनकी बाद में नेहरू खुद “विशालता की बीमारी” के रूप में आलोचना की। इसने पानी के प्रबंधन में भारत की समस्याओं को जारी रखा। बांधों पर भारी निर्भरता रही। जंगलों की उपेक्षा हुई। एक गलतफहमी बनी रही कि हम ‘प्रकृति को नियंत्रित’ कर सकते हैं।
वाटरशेड में इसका एक गौर करने लायक उदाहरण है कि कैसे केरल में वनों की कटाई ने 2018 की विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। और फिर भी, केरल के जल संसाधन विशेषज्ञों ने संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में दोषारोपण किया है कि बांधों के निर्माण के लिए जंगलों से जुड़ी क्लियरेंस देने की गति धीमी है जिसकी वजह से वे बाढ़ का बेहतर प्रबंधन नहीं कर सके!
पैसा, बिजली और पानी
जाहिर है कुछ तो गड़बड़ है। मृदुला रमेश का कहना है कि इसका अधिकांश हिस्सा अनुचित प्रोत्साहनों पर टिका है। इनमें कृषि के लिए मुफ्त बिजली है। राजनेताओं के लिए फायदेमंद यह है कि इसके प्रबंधन के बजाय बुनियादी ढांचे को महत्व दें। इस तरह राजनीतिक तौर पर पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बहुत अवहेलना हुई है। यह विनाशकारी है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के नुकसान बहुत गहरे हैं। यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीकों से विनाशकारी है, जिसमें गरीबों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। एक उदाहरण में, पुस्तक की शुरुआत में मृदुला रमेश ने सूखे का सामना कर रहे दो किसानों का वर्णन किया है। पहले किसान की, भारत के आधे किसानों की तरह, सिंचाई तक पहुंच नहीं है। उसे अपने खेतों में पौधे लगाने, पानी देने और खाद डालने के लिए उधार लेना ही है और उसे केवल नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा, जिसके पास सिंचाई का साधन है, वह भी उधार लेता है और उसकी उपज में गिरावट आती है। चूंकि सूखे की वजह से उत्पादन कम हो गया है, इससे उसकी फसल की कीमत बढ़ जाती है।
पूरे वाटरशेड में, रमेश ने दिखाया है कि इस तरह के शक्ति असंतुलन के चलते पानी से संबंधित आपदाओं के अनुभव सामने आते हैं। वे लिंग, वर्ग और जाति में नजर आते हैं। मृदुला रमेश जो समाधान प्रस्तुत करती हैं, और अगले कदम के बारे वह जो सुझाती हैं, वे न केवल भारत के जल संकट को संबोधित करने के बारे में हैं, बल्कि समानांतर चल रहे असमान अवसरों के संकट को भी सुलझाने के लिहाज से अहम हैं जो भारत के जलवायु संकट के साथ-साथ बढ़ रहा है।
उनका ध्यान मुख्य रूप से जल प्रबंधन को दमदार बनाने पर है, और वह उन प्रमुख तरीकों की पहचान करती हैं, जिनसे नागरिक समाज के प्रयास, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी इस काम में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, यहां एक निश्चित विसंगति है। किताब में वे गुजरात और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव के उदाहरण देती हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों द्वारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मीटर कनेक्शन आदि जैसे विशिष्ट प्रोत्साहनों द्वारा संचालित हैं। अनुत्तरित प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिए कोई कैसे प्रेरित करेग? और हम सहकारी संघवाद की एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कैसे करें जो भारत के साझा, लेकिन घटते पानी के प्रति बढ़ते तनाव को कम करे?





![Forest fire near Ramgarh, Uttarakhand [Image by: Joydeep Gupta]](https://dialogue.earth/content/uploads/2020/03/Forest_Fire_Ramgarh_JG-300x200.jpg)



